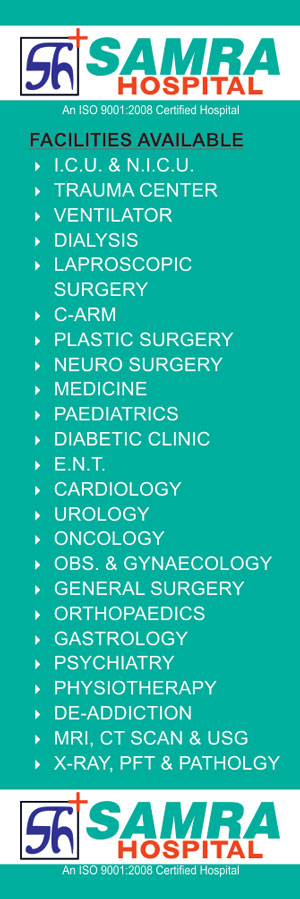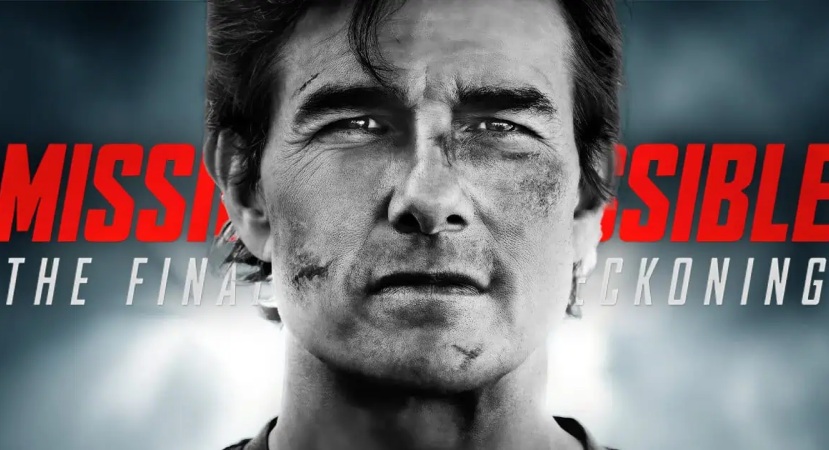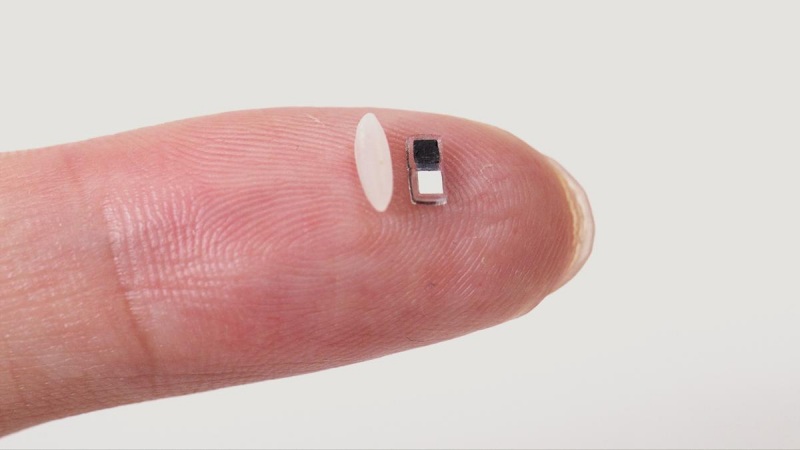लखनऊ। इमाम हुसैन की शहादत की यादगार के रूप में मनाया जाने वाला पर्व मोहर्रम नवाबीने अवध के दौर में शिया व सुन्नी मुसलमानों के अलावा हिन्दुओं में भी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के भाव से मनाया जाता था। या यूं कहा जाए कि वहीं से अवध में गंगा जमनी तहजीब की नींव पड़ी तो अतिश्योक्ति ना होगा। अवध के शिया शहंशाह और नवाबों ने 1838 में इसकी शुरूआत की थी। यहां हिंदू संस्कृति का असर भी इस पर साफ नजर आता है। lucknow muharram

अवध के पहले राजा मोहम्मद अली शाह बहादुर (1838) के जमाने में मोहर्रम का पहला शाही जुलूस निकला था। वैसे तो अवध क्षेत्र में मोहर्रम अवध की सरकार की स्थापना से पहले भी मनाया जाता था, लेकिन अवध में बुरहानुल मुल्क की हुकूमत बनने के बाद मोहर्रम को जो फरोग मिला वो पूर्व में शायद उतना नहीं था। ये नवाबों की दी हुयी गंगा जमनी तहजीब की देन ही है कि मोहर्रम मुसलमानों के अलावा हिन्दुओं और अन्य सम्प्रदाय से संबंध रखने वालों का पर्व हो गया था। अवध के शासकों, नवाबो और तमाम हिन्दू धनाढ्य व विशिष्ट वर्ग के लोगों ने यहां इमामबाड़े बनवाए। जिनमें लखनऊ में किशनू खलीफा का इमामबाड़ा, झाऊलाल का इमामबाड़ा और रायबरेली के नसीराबाद कस्बे में महाबीर का इमामबाड़ा बेहद मशहूर हुआ। इन इमामबाडों में आज भी उसी रवायत के साथ मोहर्रम मनाया जाता है और अजादारी की जाती है।
नवाबीने अवध के दौर से ही हिन्दू और मुसलमान दोनों के एक साथ त्यौहार मनाने की परंपरा कायम हुयी। उस दौर में दोनों संप्रदायों की महिलाएं एकत्र होकर शोकपूर्ण लय में नौहे गाती थीं। इन दोहों या गीतों में इमाम हुसैन एवं उनके अनुयायियों को शत्रुओं ने कितनी निर्दयता के साथ शहीद किया, इसका वर्णन अवधी भाषा में होता था। अजादारी और मातम करने वालों के लिए हिन्दू-मुस्लिम दोनों सम्प्रदाय के लोग जगह-जगह पर सबीलें लगाते थे। सबीलों की ये परंपरा आज भी कायम है।
नवाबी दौर से ही मोहर्रम के दिनों में इमाम बाड़ों में प्रकाश की विशेष व्यवस्था की जाती थी। कंदीलें और लाल एवं हरी मोमबत्तियां रौशन की जाती थीं। इस प्रकाश एवं कारचोबी के काम की चमक-दमक, सोने-चांदी के अलमों और पंजों की जगमगाहट और उनके पटकों की सजावट, जरदोजी के काम पर किरन की झालर तथा दरो-दीवार की चमक-दमक, से इमामबाड़े देखते ही बनते थे। खासकर शबे आशूर (दस मोहर्रम की रात्रि या कत्ल रात) को इमामबाड़ों की सजावट व रोशनी का प्रबन्ध इतना अधिक शानदार होता था कि देखने वालों की आखें चकाचौंध हो जाती थीं।
तत्कालीन अवध के शासक भी काले वस्त्र धारण कर, अपने सिर से ताज उतार कर उस पर ताऊस (मोर) के पर (पंख) का ताज धारण करके बैठते थे। उस समय अवध के सभी शासक मोहर्रम के लगभग सभी आयोजनों में श्रद्धा के साथ भाग लेते थे। नवाब शुजाउद्दौला बड़ी को इसमें इतनी आस्था थी कि पूरे मोहर्रम वे सोगवार रहते हुए अजादारी किया करते थे। आसिफउद्दौला के जमाने में ताजियादारी को बेहद फरोग मिला। बताया जाता है कि अक्सर ऐसा होता था कि वे खुद मातम करते-करते लहूलुहान हो जाते थे। वाजिद अली शाह मोहर्रम का चांद दिखने के बाद से हरा वस्त्र धारण कर लिया करते थे। दस मोहर्रम की रात्रि में वह जनसाधारण के घरों में जाकर ताजियों का दर्शन करते थे। मोहर्रम के जुलूस में वह स्वयं ताशा (एक तरह का बाजा) बजाया करते थे। lucknow muharram
विशेष रीतियां और जुलूस हैं खास
वैसे तो उस काल में मोहर्रम के अवसर पर अजादारी प्रारंभिक दस दिनों तक बराबर चलती रहती थी, लेकिन पहली से लेकर दस मोहर्रम तक की तिथियों में से कुछ तिथियां विशेष रीतियों एवं जुलूस के लिए खास थीं। अवध के शासकों के समय में सातवीं मोहर्रम को हजरत कासिम की (मेंहदी) शादी का जुलूस बेहद शानो शौकत से निकलता था। इसमें सबसे आगे हाथियों एवं ऊँटों की कतारें रहती थीं। आगे चल रहे सिपाही तथा बाजे वाले इमामबाड़े के सदन में बायीं ओर उचित ढंग से इस प्रकार खड़े हो जाते थे कि बीच में रास्ता बन जाता था। सबसे पहले अंदर प्रवेश पाने वाले सामान में चांदी की कश्तियों में मिठाईयां, सूखे मेवे एवं फूलों के हार होते थे।
इसके बाद झिलमिलाती पोशाक पहने सेवक सिरों पर मसहरी रखे तथा कुछ गुलदस्ते लिए हुए आते थे। इनके पीछे दुल्हन की चांदी की पालकी होती थी, जिसके संग सुंदर वर्दी धारण किये हुए मशालची कुमकुमों में प्रज्ज्वलित मशालें लिये चलते थे। दुल्हन की इस पालकी पर रुपये और चांदी के अन्य सिक्के न्योछावर किये जाते थे। कुछ लोग हजरत कासिम का ताबूत कंधों पर उठाये होते थे। पीछे-पीछे मातमी दस्ते मातमी वस्त्र धारण किये हुए प्रवेश करते थे। जो शाही दौर के खत्म होने के बाद धीरे धीरे काफी बदल चुका है। lucknow muharram
हिन्दोस्तान की देन है ताजियादारी
ताजिया भी हिन्दुस्तान की ही देन है। सबसे पहला ताजिया यहीं उठाया गया था। लोग बताते हैं कि शहंशाह तैमूरलंग प्रतिवर्ष मोहर्रम के अवसर पर इमाम हुसैन की मजार पर जाकर दर्शन करता था। भारत पर आक्रमण के दौरान युद्ध काल में ही मोहर्रम का चांद दिखाई पड़ा। उस समय उसके लिए कब्रे हुसैन पर पहुँचना असम्भव था। सलाहकारों की सलाह पर उसने इमाम हुसैन के रौजे की शबीह (प्रतिमूर्ति) बनवायी और उसके सम्मुख शोक प्रकट करके अपनी श्रद्धा और भक्ति को संतुष्ट किया। वही शबीह ताजिये की नींव (आधार) बनीं। तैमूर ने जो शबीह बनवायी थी, वह इमाम हुसैन के रौजे की हू-ब-हू नकल रही होगी, लेकिन आगे चलकर ताजिये के आकार एवं प्रकार में बदलाव आया और इसकी बनावट में हिन्दू शैली प्रदर्शित होने लगी। अवध में प्राचीन समय में जो ताजिये प्रचलित थे, उनका गुम्बद हिन्दुओं के मंदिर से मिलता-जुलता होता था। lucknow muharram
अवध के शासकों के काल में मोहर्रम के पर्व में भारतीय एवं हिन्दुओं के प्रभाव की छाप स्पष्ट रूप से मिलती है। उस समय हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा मोहर्रम को मनाने का जो ढंग था उसने एक ओर तो खुद इस पर्व के संयुक्त सांस्कृतिक रूप को निखारा तथा दूसरी ओर इससे अवध की सांझी संस्कृति को भी बड़ी शक्ति मिली।
# lucknow muharram